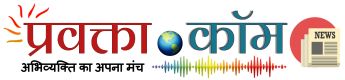1987 से 2020 तक दिल्ली में 33 साल रहने के बाद जब मैं गांव में स्थायी रूप से रहने के लिए आया तो मैंने महसूस किया कि गांव अब मेरे लिए उतना जाना-पहचाना नहीं है। 40 वर्ष से कम उम्र के अधिकतर लोगों को मैं नहीं जानता था। हालांकि दशहरा वाले कार्यक्रम के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ। मैं प्रायः पूछता और शायद मेरे बारे में भी लोग पूछते, “ये किसके घर के हैं।” ‘घर’ एक ऐसा माध्यम था जिसके सहारे किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी को अपडेट करना बहुत सहज और आसान था।
जल्दी ही गांव में सभी लोग मुझे जान गए। लेकिन अभी ‘पहचान’ बाकी थी। वास्तव में ‘पहचान’ एक वृक्ष जैसी होती है। इसकी शुरूआत बीज से झांकते अंकुर के रूप में होती है। धीरे-धीरे इसमें पत्तियां आती हैं, एक डंठल नुमा कोमल तना बनता है और फिर कई सालों में शाखाओं, प्रशाखाओं के साथ वह क्रमशः पूर्ण रूप में दृश्यमान होता है। यदि मैं गांव में रहता तो लोग मुझे अब तक अच्छे से ‘पहचान’ चुके होते, लेकिन यहां तो 33 वर्षों का अंतराल था। इस अंतराल के कारण जो ‘पहचान’ का संकट था, उसे दूर करना बहुत जरूरी था।
जो ‘पहचान’ 33 वर्षों में धीरे-धीरे बनती, उसे अब कुछ महीनों में आकार देना था। मुझे अपने साथ-साथ गोविन्दाचार्य जी और मिशन तिरहुतीपुर की भी गांव में ‘पहचान’ करवानी थी। बात केवल जानकारी देने भर की होती तो मुझे कोई समस्या नहीं थी। मेरे पास अगले 7 वर्षों का रोडमैप तैयार रखा हुआ था। 654 पेज के इस रोडमैप में 9 सेक्टर और 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स के साथ हर छोटी-बड़ी बात विस्तार से लिखी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य से गांव में ‘पहचान’ बनाने की दृष्टि से इसकी कोई खास उपयोगिता नहीं थी।
अपनी ‘पहचान’ बनाने के साथ-साथ मुझे गांव के साफ्टवेयर पर भी काम करना था, अर्थात लोगों की मानसिकता में आवश्यक बदलाव करना था। यही मेरा मुख्य काम था। इसीलिए मैं गांव आया था। लेकिन ये दोनों काम बतला कर, भाषण देकर या समझा कर संभव नहीं थे। ऐसा करने का उल्टा असर हो सकता था। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे बैकफायर इफेक्ट कहते हैं। इसके अनुसार जब हम किसी व्यक्ति की मान्यता, विश्वास या आदत को तार्किक आधार पर बदलने का प्रयास करते हैं तो वह उन्हें छोड़ने की बजाए प्रायः और कस कर पकड़ लेता है और फिर पूरी ताकत लगाकर उन्हें उचित ठहराने की कोशिश करता है।
कई शहरी लोग जो कुछ अच्छा करने की नीयत से गांव आते हैं, वे प्रायः इस बात को नहीं समझ पाते। वे गांव को तर्क के आधार पर जितना बदलने की कोशिश करते हैं, गांव उतना ही उनके प्रति लापरवाह होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वे गांव वालों को कोसना शुरू कर देते हैं और गांव वाले उनका मजाक उड़ाने में लग जाते हैं। अंत में थक-हार कर उन्हें या तो गांव छोड़ वापस शहर जाना पड़ता है या फिर गांव में ही चुपचाप एकाकी जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ता है।
मैं नहीं चाहता था कि मेरा भी यही हस्र हो, इसलिए मैंने किसी को उपदेश देने या समझाने से तोबा कर ली थी। मैंने तय किया था कि लोगों को बदलने के लिए मैं उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करूंगा जिनका इस्तेमाल करके प्रायः लोगों को बिगाड़ा जाता है। इस मामले में मैंने Edward Bernays से सीखने की कोशिश की। यह वही एडवर्ड बर्नेज है जिसे आज पी.आर. और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री अपना जनक मानती है। किसी मुद्दे पर लोगों का नजरिया बदलना उसे बहुत अच्छे से आता था।
1929 में बर्नेज ने एक ऐसा कारनामा किया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। उस समय अमेरिका में आदमियों का सिगरेट पीना आम बात थी। लेकिन औरतों का सरेआम सिगरेट पीना तब तक वहां भी बुरा माना जाता था। सिगरेट कंपनियां इस स्थिति को बदलना चाह रही थीं। उनकी कोशिश थी कि औरतों में भी सिगरेट पीना फैशन की बात बन जाए। कई कोशिशों के बाद भी जब यह नहीं हो पाया तब अमेरिकन टोबैको कंपनी ने एडवर्ड बर्नेज को काम पर लगाया। बर्नेज ने मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी चाल चली कि कुछ ही समय में अमरीकी महिलाओं में सिगरेट पीना रूतबे और सम्मान की बात हो गई।
हुआ यह कि बर्नेज ने कुछ महिला मॉडल्स को पैसे देकर इस बात के लिए राजी किया कि वे न्यूयार्क की मशहूर ईस्टर परेड में खुलेआम सिगरेट पीते हुए चहल-कदमी करें। इस घटना को उसने “Torches of Freedom” के नाम से मीडिया में खूब प्रचारित किया। कहा गया कि सरेआम सिगरेट पीने से एक महिला उस व्यवस्था को चुनौती देती है जो पुरुष के सिगरेट पीने को फैशनेबल किंतु महिला के सिगरेट पीने को हेय मानती है। सिगरेट को आजादी की मशाल बताया गया जिसे सुलगाते ही महिला पुरुषों की बराबरी में खड़ी हो जाती है। इस अभियान को अमेरिका की तत्कालीन फेमिनिस्ट आंदोलनकारियों का भरपूर समर्थन मिला।
कहने की बात नहीं कि इस कैंपेन के बाद सिगरेट की बिक्री में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुई। बर्नेज के ऐसे कई और कारनामें हैं जहां उसने कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। मनोविज्ञान के इस्तेमाल से मुनाफा कमाने की संभावना पर आगे और भी बहुत काम हुआ। धीरे-धीरे अर्थशास्त्र में एक नई शाखा ही विकसित हो गई जिसे नाम दिया गया बिहेवियरल एकोनामिक्स। 2002 में एक मनोवैज्ञानिक Daniel Kahneman को इसी क्षेत्र में काम के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
डेनियल काह्नमैन की एक मशहूर किताब है जिसका नाम है- Thinking Fast and Slow. इसके अनुसार मानव मष्तिष्क कोई निर्णय लेने में दो तरह के सिस्टम का उपयोग करता है – सिस्टम-1 और सिस्टम-2. जब भी कोई निर्णय लेने की बात आती है तो सबसे पहले सिस्टम-1 को जिम्मेदारी मिलती है। सिस्टम-1 बहुत चौकन्ना और तेज होता है। किसी बात पर फैसला लेने में इसे एक सेकंड से भी कम समय लगता है। कोई बात जब सिस्टम-1 को तुरंत समझ में नहीं आतीं, तो यह फैसला लेने का काम सिस्टम-2 को सौंप देता है। सिस्टम-2 धीरे-धीरे लेकिन सोच-समझ कर फैसला लेता है। सिस्टम-2 तर्क से चलता है जबकि सिस्टम-1 भावना से संचालित होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि सिस्टम-2 तभी फैसला लेता है जब ऐसा करने के लिए उसे सिस्टम-1 की ओर से कहा जाए। विडंबना यह है कि सिस्टम-2 अपनी ओर से पहल करके कभी कोई निर्णय नहीं लेता। कहने का मतलब यह है कि जब आपको अपनी कोई बात किसी को समझानी हो तो सबसे पहले उसके सिस्टम-1 से बात करिए। विज्ञापन जगत में यही होता है।
बिहैवियरल एकोनामिक्स, मनोविज्ञान और काग्निटिव साइंस के सभी सिद्धांत दुधारी तलवार के समान हैं। इनसे जहां लोगों को बिगाड़ा जा सकता है तो वहीं इनका इस्तेमाल करके समाज सुधार भी हो सकता है। दुर्भाग्य से समाज को बिगाड़ने वाले इनका इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं, जबकि समाज का भला चाहने वाले कमोबेश इनसे बेखबर हैं। मेरी कोशिश है कि मिशन तिरहुतीपुर इस मामले में एक छोटा ही सही लेकिन मजबूत कदम उठाए।
इस डायरी में फिलहाल इतना ही। आगे की बात हम डायरी के अगले अंक में करेंगे, इसी दिन इसी समय, रविवार 12 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
विमल कुमार सिंह
संयोजक, मिशन तिरहुतीपुर