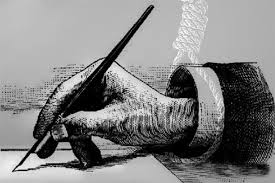मनोज कुमार
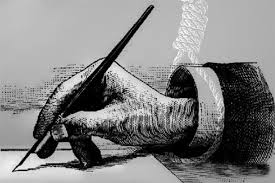
शब्द सत्ता की शताब्दी मनाते हुए हम हर्षित हैं लेकिन यह हर्ष क्षणिक है क्योंकि महात्मा गांधी जैसे कालजयी नायक के डेढ़ सौ वर्षों को हम चंद महीनों के उत्सव में बदल कर भूल जाते हैं, तब सत्ता को आहत करने वाली पत्रकारिता की जयकारा होती रहे, यह कल्पना से बाहर है। इन सबके बावजूद शब्द की सत्ता कभी खत्म नहीं होने वाली है और ना ही उसकी लालसा स्वयं के जयकारा करने में है। शब्द सत्ता तो दादा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता का वह गान है जिसमें दादा लिखते हैं..चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं..चाह नहीं.. इसी तरह शब्द सत्ता के माध्यम से संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर शब्द सत्ता के माध्यम से समतामूलक समाज के लिए संघर्ष करते हैं। शब्द सत्ता की महत्ता तो तब है कि उसके लिखे से देश, प्रदेश और समाज की परिस्थिति में परिवर्तन आए। वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। वह स्व के स्थान पर परहित में स्वयं की कामयाबी देखता है। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित पत्रिका ‘कर्मवीर’ का विवेचन करते हैं या फिर डॉ. अम्बेडकर द्वारा सम्पादित ‘मूक नायक’ का अध्ययन करते हैं तो पत्रकारिता का ध्येय स्पष्ट हो जाता है। स्वाधीनता भारत में ‘कर्मवीर’ ने लोक जागरण का आह्वान किया था तो डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी ‘मूक नायक’ के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता के खिलाफ लड़ते रहे। यह संयोग है कि एक पखवाड़े के अंतराल में दो महनीय प्रकाशनों के सौ वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस बात को कहने में संकोच नहीं है कि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात कर्मवीर और मूकनायक जैसे प्रकाशन विस्मृत हो चले हैं। स्मरण नहीं आता कि स्वाधीन भारत में इन दोनों प्रकाशनों में प्रकाशित होने वाली किसी सामग्री से सत्ताधीश असहज हुए हैं। क्योंकि इन प्रकाशनों में वह धार अब शेष नहीं है जिसकी पत्रकारिता से उम्मीद की जाती है। पराधीन भारत में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ अनेक देशप्रेमी पत्रकार रहे लेकिन यहां चर्चा कर्मवीर और मूक नायक की क्योंकि 2020 में इनके प्रकाशन के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। कर्मवीर और मूक नायक की चर्चा करते समय हमें इस बात के लिए चिंता करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कर्मवीर, मूक कब हो गया? क्यों हमने उसे राष्ट्र की आवाज बनाने की कोशिश नहीं की। जितना और जहां तक मेरा अनुभव है प्रकाशन सरकारों की जयकारा नहीं करती है। यदि ऐसा होता तो अंग्रेज शासकों को कर्मवीर के नाम पर पसीना नहीं छूटा करता। फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्मवीर से नई पीढ़ी का परिचय ही नहीं है। मूक नायक के प्रभावों से आने वाली पीढ़ी अनजान है। यह बात भी सौफीसदी सच है कि स्वाधीनता के बाद नव भारत के निर्माण की महती जिम्मेदारी पत्रकारिता के कंधे पर थी और पत्रकारिता ने इस जवाबदारी को, पत्रकारिता के धर्म को बखूबी निभाया लेकिन जैसे जैसे स्वराज से सुराज की तरफ हम चल पड़े, पत्रकारिता की तेजहीन होने लगा। खासतौर पर 1975 के आपातकाल के बाद तो जैसे पत्रकारिता इस या उस खेमे में बंट गया। पत्रकारिता की रीढ़ की हड्डी कमजोर होने लगी लेकिन पत्रकारिता कुनबे को इस बात से गौरव हो सकता है कि इस संक्रमणकाल में भी नईदुनिया, इंदौर जैसा प्रकाशन ने अपनी रीढ़ को वैसे ही मजबूत रखा। यह पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 1975 के आपातकाल के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पत्रकारिता का हुआ। इसी दौर में प्रकाशनों की बाढ़ सी आ गई। अनेक राज्यों में कई नए प्रकाशनों का आरंभ हुआ तो कई पुराने प्रकाशनों ने राज्य और जिला संस्करण आरंभ कर उन्हें विस्तार दिया। इस विस्तार से प्रकाशन संस्थान और समाज दोनों को लाभ हुआ। शासन और सत्ता तक आंचलिक समस्याओं की सूचना पहुंचने लगी और समस्याओंं का निपटारा तेज गति से होने लगा। दूसरी तरफ महानगरों में होने वाली गतिविधियों एवं नवाचार से वंचित तबका अब जानकारी से परिपूर्ण था। प्रकाशनों के विस्तार का लाभ तो यह हुआ लेकिन एक बड़ा नुकसान यह भी हुआ कि प्रशिक्षण के अभाव में ऐसे लोगों को पत्रकार के रूप में स्थापित कर दिया गया जिन्हें इस विधा की समझ तो दूर, उन्हें पर्याप्त अक्षर ज्ञान भी नहीं था। इस कारण कई बार विषम स्थिति बनती गई। निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रकाशनों को माध्यम बनाये जाने की कई घटनाएं सामने आने लगी। प्रकाशनों ने ऐसे पत्रकारों के लिए आय के स्रोत के नाम पर विज्ञापन संग्रहण की जिम्मेदारी सौंप दी गई। विज्ञापनदाता भी इसका अनुचित लाभ लेेने लगे। अपने पक्ष में ऐसी खबरें छपवा लेते जिसका जमीनी स्तर पर कोई वास्ता नहीं होता था। 70 से 80 के दशक के मध्य इस तरह का व्यवहार तेजी से पनपा। इसे तब पीत पत्रकारिता संबोधित किया गया। पीत पत्रकारिता से अर्थ वही था जिसे आज हम पेडन्यूज कहते हैं। पीत पत्रकारिता से पेडन्यूज का यह सफर पत्रकारिता को नेपथ्य में ले जाकर मीडिया में रूपांतरित करने का काल है।
इस कालखंड में टेलीविजन का उद्भव होता है। साल 75 में हम पत्रकारिता के जिस उत्तरदायित्वहीनता की चर्चा करते हैं, वह 90 के दशक में ठसक के साथ व्यवहारित होता दिखता है। उम्मीदें थी कि टेलीविजन की पत्रकारिता समाज को नया दिशा देगी लेकिन उम्मीदें धराशायी हो गई। कयास यह भी लगाया गया था कि टेलीविजन के आगमन से प्रकाशन बंद हो जाएंगे लेकिन हुआ उल्टा। करीब तीन दशक में ही लोगों का टेलीविजन पत्रकारिता से मोहभंग हो गया। टेलीविजन पत्रकारिता पर कई किस्म के सवालिया निशान लगे। साफतौर पर टेलीविजन पत्रकारिता ने वह मार्ग चुना, जिसके लिए प्रिंट पत्रकारिता को वर्षों लगने के बाद भी वह स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाया। प्रकाशनों पर समाज का विश्वास और गहराया है।प्रकाशन रंगीन ना होकर श्वेत-श्याम हो लेकिन उसकी छाप, उसके शब्दों का असर दूरगामी होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से जो बात हम लगातार कहते चले आ रहे हैं कि पत्रकारिता को मीडिया में परिवर्तित कर दिया गया है. पत्रकारिता तब से लेकर अब तक ध्येयनिष्ठ है जबकि दो दशकों में पनपने वाला मीडिया लक्ष्य निष्ठ है. ध्येय क्या है, यह बताने की जरूरत नहीं, वैसे ही लक्ष्य क्या है, यह भी बताने की जरूरत शायद नहीं है क्योंकि ध्येय दूरगामी परिणाम देने वाला होता है और यह पत्रकारिता के हिस्से में है जबकि लक्ष्य स्वहित की चर्चा करता है, इसलिए इसका प्रभाव तात्कालिक होता है. सौ साल बाद हम कर्मवीर और मूक नायक की चर्चा कर रहे हैं तो साफ है कि यह ध्येयनिष्ठ अर्थात पत्रकारिता का उदाहरण है लेकिन सौ साल बाद हमारी बाद की पीढ़ी, किसी मीडिया की मीमांसा करेगी, यह संभव नहीं दिखता है. ऐसे समय में कर्मवीर और मूक नायक का स्मरण किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है।
यह आवश्यक इसलिए भी है कि प्रकाशनों की भीड़ बढ़ती जा रही है लेकिन कटेंट में वह मारक क्षमता नहीं है जो सत्ता की नींद में खलल डाल सके। पाठक और समाज बहुत संजीदगी से प्रकाशनों को देख रहा है कि इस समय में हमारी जवाबदारी बढ़ चुकी है। एक बात पर करार किया जा सकता है, समझौता हो सकता है कि आज के दौर में कर्मवीर और मूक नायक का प्रकाशन नहीं हो सकता है लेकिन इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश की सत्ता के गीत गाएंगे, टेलीविजन की तरह प्रकाशनों को भी असामायिक बना देेगी। पेज-थ्री की पत्रकारिता करना हो तो इसे मीडिया कहना ही उचित है लेकिन गांधी-तिलक की पत्रकारिता करना हो तो कर्मवीर बनना पड़ेगा। मूक युग में प्रवेश करती सत्ता और उसे मठाधीशों को आईना दिखाना होगा। सोशल मीडिया ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि उसका प्रभाव तो खूब है लेकिन स्वछंदता उसे अनियंत्रित कर देता है जिससे समाज में एक किस्म की अराजकता उत्पन्न होती है। पत्रकारिता शुचिता और शुभ की मंगलकामना करती है जबकि मीडिया स्वयं के गीत गाने में मगन रहती है। 100 साल के कर्मवीर और मूक नायक अपने आरंभ से अब तक और आगे भी समाज शुचिता और शुभ की मंगलकामना करती रहेगी।